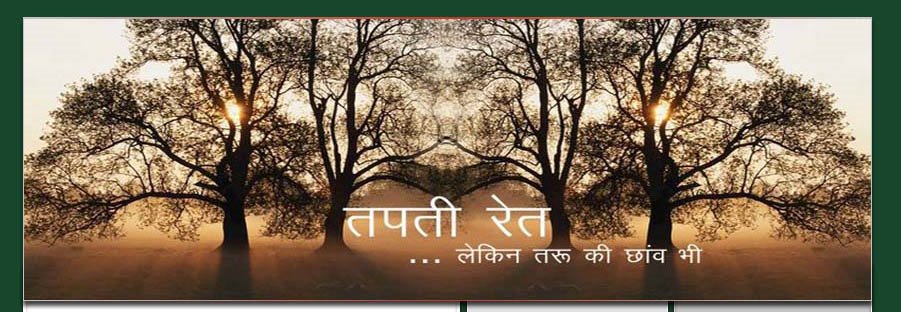दिल्ली की ठंडी शाम थी और महज चार घंटे बाद ट्रेन। मैं, मेरी बहिन और उसकी फ्रेंड सहित हम चार लोग थे और करोल बाग के बाजार में शॉपिंग के बाद एक और दोस्त को साथ लेकर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना था। इसके बाद राजेन्द्र प्लेस की एक होटल से अपना सामान उठाकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने तक की पूरी कवायद दिमाग में चल रही थी। शॉपिंग पूरी होते होते लगभग दो घंटे बीत गए थे और निकलने के समय कपड़ों की ऑल्टरेशन में लगभग 20 मिनट लगने की बात स्टोर कीपर ने कह दी थी। सोचा, तब तक अपने साथ के एक मित्र को बाहर से कुछ औऱ शॉपिंग करनी बाकी रह गई थी सो वही करा दी जाए। आखिर टाइम मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान केंद्रित था। बाहर आ कर खरीददारी करने में बमुश्किल सात आठ मिनट लगे कि तभी गोल गप्पे वाला दिख गया। बस... फिर क्या था, गोल गप्पे वाला दिखे और मैं गोल गप्पे ना खाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता ना। सारा सामान उठाकर गोलगप्पे वाले के पास पहुंच गए। इस खाने पीने से निवृत्त होते तब तक पन्द्रह मिनट बीत चुके थे। सो सारा सामान अपने साथ के लोगों के हवाले छोड़कर मैं कपड़े लेने स्टोर पहुंच गई। कपड़े तैयार थे, फटाफट लिए और तब तक सभी लोग बाहर आकर मेरा ही इंतजार कर रहे थे। खाना खाने के लिए साथ आने वाला मित्र भी पहुंच चुका था और हमें निर्धारित स्थान पर पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा ही सबसे उचित साधन लगा। तो बस ऑटो में सवार होकर सभी निर्धारित स्थान पहुंचे कि तभी ध्यान आय़ा...
उफ्फ....मेरा पर्स कहां है?
तभी ध्यान आया कि शायद गोलगप्पे वाले के पीछे खड़ी कार पर ही छूट गया हो। अब क्या किया जाए...
ट्रेन छूटने में महज डेढ़ घंटा बाकी था। बहिन और उसकी फ्रेंड ने कहा हम लोग ढूंढ लाते हैं तब तक आप लोग जाकर खाना ऑर्डर करो... जब तक ऑर्डर पूरा होगा....हम लौट आएंगे।
आईडिया बढ़िया था सो हम लोग दो भागों में बंट गए। खाने का ऑर्डर तो किया लेकिन मन खाने में कम पर्स में ही ज्यादा था। तभी फोन आ गया कि पर्स गोलगप्पे वाले के यहीं मिल गया है और बाकी की सारी कहानी वहां आकर बताते हैं। थोड़ी सांस आई। खाना आने तक वे लोग लौट आए थे। खाना खाते खाते बात हुई...
गोलगप्पे वाले ने पर्स में बम समझकर उसे दूर कम भीड़ भाड़ वाले स्थान पर रख दिया था। पुलिस को इत्तिला इसलिए नहीं दी कि कल से उसका ठेला वहां लगने नहीं देंगे। इन लोगों के जाते ही वो जैसे उबल पड़ा।
ध्यान क्यों नही रखते हैं आप लोग... मेरी रोजी पर संकट आ जाता आप लोगों की वजह से। और भी बहुत कुछ....
शायद इसीलिए कहते हों कि डर के आगे जीत है।
क्या करते, सब कुछ सुनते रहे चुपचाप। आखिर पर्स मिल गया था.... चुपचाप सारी बातें सुनकर और उसे धन्यवाद कहते हुए ये लोग लौट आए। काम निपटा कर सही वक्त पर स्टेशन पहुंचे और ट्रेन भी पकड़ ली। तब कुछ सोचने का वक्त मिल पाया....
इतने भीड़ वाले इलाके से पर्स मिलना नामुमकिन सा लग रहा था... लेकिन मिल गया। खुशी बेहद हुई पर सवालों ने दुखी कर दिया....
अगर वह वास्तव में मेरा पर्स नहीं किसी आतंककारी का रखा बम होता तो कितनी जानें लेता?
मेरे देश का आम आदमी किस दहशत में जिंदगी बसर कर रहा है?
संवेदना भूख पर हमेशा भारी पड़ती है। आम आदमी बेचारा अपनी दो समय की रोटी कमाने के बीच इतना कहां सोच पाता? पर्स देखते ही उसे अपनी बीवी बच्चों की शक्ल याद आई होगी। बम हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ऊहापोह में कुछ देर रहा होगा। देश के कानूनी फेर याद आए होंगे और ऐसे में विस्फोट में मरने वालों से ज्यादा खुद ही की चिंता होना लाजिमी था।
कुछ ऐसी ही भूख होती होगी वो जो एक आम आदमी को संवेदनहीन आतंककारी में तब्दील करती होगी....क्या कहते हैं आप?